बायें से वे मलते हुए पेट को चलते,
और दाहिना दया दृष्टि-पाने की ओर बढ़ाये।
भूख से सूख ओठ जब जाते
दाता-भाग्य विधाता से क्या पाते?--
घूँट आँसुओं के पीकर रह जाते।
चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए,
और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए!
कुंडलियाँ
गिरिधर कविराय
परिचय :
* गिरिधर कविराय, हिंदी के प्रख्यात कवि थे।
निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :
१.लाठी में हैं गुण बहुत, सदा रखिये संग।
गहरि नदी, नाली जहाँ, तहाँ बचावै अंग।।
तहाँ बचावै अंग, झपटि कुत्ता कहँ मारे।
दुश्मन दावागीर होय, तिनहूँ को झारै।।
कह गिरिधर कविराय, सुनो हे दूर के बाठी।
सब हथियार छाँडि, हाथ महँ लीजै लाठी।।
कमरी थोरे दाम की, बहुतै आवै काम।
खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखै मान॥उनकर राखै मान, बँद जहँ आड़े आवै।
बकुचा बाँधे मोट, राति को झारि बिछावै॥
कह ‘गिरिधर कविराय’, मिलत है थोरे दमरी।
सब दिन राखै साथ, बड़ी मर्यादा कमरी॥
क) गिरिधर कविराय जी ने लाठी की किन-किन गुणों की ओर संकेत
किया है ?
: कविराय जी ने लाठी के कई गुणों की ओर संकेत किया है।लाठी अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती
है। कहीं गड्ढा आ जाए, तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है, कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग
करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा
सकता है। यदि मार्ग में कुत्ते या चोर या फिर डकैत आक्रमण कर दे तो, लाठी उन सभी से हमारी रक्षा करती
है और उन पर विजय भी दिलाती है।
ख) कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कह रहे हैं। क्या आप उनकी बात से
सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।
: कवि गिरिधर जी ने सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात कह रहे हैं। मैं उनकी बात
से सहमत हूँ क्योंकि, पुराने समय में अधिकतर लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इस यात्रा में उन्हें कई मुश्किलों
का सामना करना पड़ता था जैसे गहरी नदी या नाला पार करना और हिंसक जानवरों और दुश्मनों से अपनी
सुरक्षा करना।लाठी, यात्री को इन सभी मुश्किलों में सहारा देती है।
ग) गिरिधर कविराय के अनुसार कमरी में कौन-कौन-सी विशेषताएँ होती हैं?
: कवि के अनुसार कमरी अर्थात् कंबल बहुत ही कम दाम में मिलती है परंतु यह बहुत बड़े काम आती है।
इसकी गठरी बनाकर इसमें हम अपनी कीमती वस्त्रों को सुरक्षित रख सकते हैं, यात्रा के दौरान यदि हमें
रात गुज़ारने की जगह न मिले तो, कंबल बिछाकर हम आराम से रात गुज़ार सकते हैं।
घ) रेखांकित पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं?
: रेखांकित पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि, श्रेष्ठ प्रकार के कपड़े जो यात्री अपने साथ यात्रा के
दौरान रखते हैं ताकि उन्हें यात्रा के दौरान जब उन कीमती कपड़ों की ज़रूरत पड़े तब वे उनका प्रयोग
कर अपनी इज़्ज़त को बचा सकें। कवि के अनुसार कम कीमत पर मिलने वाली इसी कंबल की गठरी
बनाकर यात्री उसमें अपने कीमती वस्त्रों को आँधी से सुरक्षित रख पाते हैं।
२. गुन के गाहक सहस, नर बिन गुन लहै न कोय।
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय॥
शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन।
दोऊ के एक रंग, काग सब भये अपावन॥
कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के।
बिनु गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक गुन के॥
साँई सब संसार में, मतलब का व्यवहार।
जब लग पैसा गाँठ में, तब लग ताको यार॥
तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले।
पैसा रहे न पास, यार मुख से नहिं बोले॥
कह गिरिधर कविराय जगत यहि लेखा भाई।
करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साँई॥
क) ‘गुन के गाहक सहस, नर बिन गुन लहै न कोय’ – पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
: प्रस्तुत पंक्ति में गिरिधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग
स्वीकार करने को तैयार रहते हैं लेकिन बिना गुणों के समाज में उसकी कोई मह्त्ता नहीं। इसलिए व्यक्ति
को अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए।
ख) कौए और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि क्या स्पष्ट करते हैं?
:कौए और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते है कि जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप-रंग में समान
होते हैं किन्तु दोनों की वाणी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह
सबको प्रिय है। वहीं दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है। अत: कवि कहते हैं
कि बिना गुणों के समाज में व्यक्ति का कोई नहीं। इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए।
ग) संसार में किस प्रकार का व्यवहार प्रचलित है ?
:कवि कहते हैं कि संसार में बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा- संबंधी नहीं होता। सब अपने मतलब के लिए
ही व्यवहार रखते हैं। अत:इस संसार में मतलब का व्यवहार प्रचलित है।
घ) उपर्युक्त कुंडलिया में सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान बताई गई है ?
: उपर्युक्त कुंडलिया के अनुसार एक सच्चा मित्र कभी अपने मित्र का मुश्किलों में कभी साथ नहीं छोड़ता है।
मित्र के प्रति उसका व्यवहार निस्वार्थ भाव से पूर्ण होता है। कवि के अनुसार एक झूठा मित्र तब तक आपका
साथ देता है, जब तक आपके पास धन - दौलत है, जैसे ही आप निर्धन हो जाते हैं वही दोस्त आपसे मुँह
फेर लेते हैं और बात तक नहीं करते हैं।
वह जन्मभूमि मेरी
सोहनलाल द्विवेदी
कवि परिचय: सोहनलाल द्विवेदी आधुनिक काल के कवि हैं।रचनाएँ - 'भैरवी, 'वासवदत्ता, 'पूजागीत, 'विषपान और 'जय गाँधी आदि। इनके कई बाल काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए।
१. जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता,/ श्रीकृष्ण ने सुनाई, वंशी पुनीत गीता।/ गौतम ने जन्म लेकर, जिसका सुयश बढ़ाया,/ जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया।
क) गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय दें।
- गौतम बुद्ध महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे।[
ख) भगवान बुद्ध ने लोगों को किस मार्ग का उपदेश दिया ? स्पष्ट करें।
इनकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ-साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों की भी प्रचुरता है।
कठिन शब्दार्थ
गति - रफ़्तार
विराम - आराम, विश्राम
पथिक - राही
अवरुद्ध - रुका हुआ
आठों याम - आठों पहर
विशद - विस्तृत
प्रवाह - बहाव
वाम - विरुद्ध
रोड़ा - रुकावट
अभिराम - सुखद
पाता कभी, खोता कभी
आशा-निराशा से घिरा
हँसता कभी रोता कभी।
गति-मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है।
चलना हमारा काम है।
किसको नहीं बहना पड़ा
सुख-दुख हमारी ही तरह
किसको नहीं सहना पड़ा।
फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूँ मुझ पर विधाता वाम है
चलना हमारा काम है।
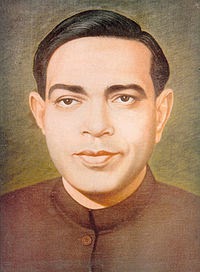
कवि परिचय:
रचनाएँ: उर्वशी (भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार) कुरुक्षेत्र, हुँकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि।
शब्दार्थ
१.धर्मराज- युधिष्ठिर
प्रश्नोत्तर
१.लेकिन विघ्न अनेक अभी
क) प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है तथा इसके रचनाकार कौन हैं ?
ख) प्रस्तुत पंक्तियों में किस विघ्न की बात कवि कर रहे हैं ?
ग) इस प्रकार के विघ्न के हटने पर क्या होगा ?
घ) आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए आप क्या करते हैं ?
२. सब हो सकते तुष्ट एक सा
क) 'तुष्ट’ शब्द से क्या तात्पर्य है ?
ख) रेखांकित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए।
ग) शब्दार्थ लिखिए:-
घ) स्वर्ग से क्या तात्पर्य है ?
३. जब तक मनुज-मनुज का यह
क) 'कोलाहल’ शब्द का अर्थ बताते हुए बताएँ कि यह अंश कवि की किस रचना से उद्धृत है ?
ख) प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन किससे कहता है ?
ग) संघर्ष कब कम नहीं होगा ? सपष्ट करें।
घ) कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे।
१. प्रस्तुत अंश कवि की किस रचना से ली गई है ?
गीध: गीध अर्थात गिद्ध से कवि का तात्पर्य जटायु से है। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो सीता की दुख भरी वाणी सुनकर जटायु ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया। सीता को खोजते हुए राम जब वहाँ पहुँचे तो उसने उन्हें रावण के विषय में सूचना देकर राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जटायु ने सीता की रक्षा करने में अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। सबरी: सबरी अर्थात शबरी एक वनवासी शबर जाति की स्त्री थी जिसको पूर्वाभास हो गया था कि राम उसी वन के रास्ते से जाएँगे जहाँ वह रहती थी। उनके स्वागत के लिए उसने चख-चख कर मीठे बेर जमा किए थे। राम ने उसका आतिथ्य स्वीकार किया और उसे परम गति प्रदान की। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था । श्रमणा भील समुदाय की "शबरी " जाति से सम्बंधित थी । संभवतः इसी कारण श्रमणा को शबरी नाम दिया गया था । पौराणिक संदर्भों के अनुसार श्रमणा एक कुलीन हृदय की प्रभु राम की एक अनन्य भक्त थी लेकिन उसका विवाह एक दुराचारी और अत्याचारी व्यक्ति से हुआ था । प्रारम्भ में श्रमणा ने अपने पति के आचार-विचार बदलने की बहुत चेष्टा की , लेकिन उसके पति के पशु संस्कार इतने प्रबल थे की श्रमणा को उसमें सफलता नहीं मिली । कालांतर में अपने पति के कुसंस्कारों और अत्याचारों से तंग आकर श्रमणा ने ऋषि मातंग के आश्रम में शरण ली । आश्रम में श्रमणा श्रीराम का भजन और ऋषियों की सेवा-सुश्रुषा करती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शबरी ने बड़े भोलेपन से प्रेमपूर्वक राम को अपने चखे हुए मीठे बेर खिलाए थे। उसके इसी प्रेमपूर्वक व्यवहार से राम प्रसन्न होकर उसे परम गति प्रदान किया। |
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु, भरत महतारी |
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितन्हि,भए-मुद मंगलकारी ||
नाते नेह राम के मनियत, सुहुद सुसैब्य जहाँ लौं |
अंजन कहा आंख जेहि फूटै, बहु तक कहौ कहाँ लौं ||
तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो |
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ||(विनयपत्रिका -१७४ )
बलि: बलि नामक दैत्य गुरु भक्त प्रतापी और वीर राजा था। देवता उसे नष्ट करने में असमर्थ थे। वह विष्णु भक्त था। एक बार राजा बलि ने देवताओं पर चढ़ाई करके इन्द्रलोक पर अधिकार कर लिया। उसके दान के चर्चे सर्वत्र होने लगे। तब विष्णु वामन अंगुल का वेश धारण करके राजा बलि से दान माँगने जा पहुँचे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सचेत किया कि तेरे द्वार पर दान माँगने स्वयं विष्णु भगवान पधारे हैं। उन्हें दान मत दे बैठना, परन्तु राजा बलि उनकी बात नहीं माना। उसने इसे अपना सौभाग्य समझा कि भगवान उसके द्वार पर भिक्षा माँगने आए हैं। तब विष्णु ने बलि से तीन पग भूमि माँगी। राजा बलि ने संकल्प करके भूमि दान कर दी। विष्णु ने अपना विराट रूप धारण करके दो पगों में तीनों लोक नाप लिया और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। |
कठिन शब्द | सरल अर्थ |
औद्योगिक - | उद्योग से संबंधित |
चकाचौंध - | तेज रोशनी या दिखाव |
संवेदनशील - | भावनाओं को जल्दी समझने वाला |
विक्षिप्तता - | पागलपन या मानसिक असंतुलन |
नग्न - | बिना कपड़ों के, खुला हुआ |
दिशाहीन - | जिसकी कोई दिशा न हो |
भीड़ - | बहुत सारे लोग एक साथ |
खोया - | गुम हो गया, अपने में नहीं रहा |
कहानीकार का परिचय:
लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) के किसान परिवार में हुआ था। वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और प्रेमचंद के उपन्यासों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। काशी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने हिंदी समिति से जुड़कर महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी लेखन शैली सरल और सुबोध है, और उनकी रचनाएँ कथा और रिपोर्ताज शैली में लिखी गई हैं। उनकी प्रमुख रचनाएँ 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' और 'स्वतंत्रता की पूर्व संध्या' हैं।
कहानी का उद्देश्य:
कहानी का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना है। यदि मनुष्य इस पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, तो वह दिन दूर नहीं जब हम सब इस बढ़ती भीड़ और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएँगे। यह कहानी हमें परिवार के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता और समाज की खुशहाली के लिए सोचने की प्रेरणा देती है।
1. लीलाधर शर्मा पर्वतीय का जन्म कहाँ हुआ था?
(a) दिल्ली
(b) अल्मोड़ा
(c) वाराणसी
(d) लखनऊ
Correct Answer : (b) अल्मोड़ा
2. लीलाधर शर्मा पर्वतीय के कौन से दो प्रमुख रचनाएँ हैं?
(a) संग्राम और आत्मकथा
(b) संयुक्त राष्ट्र-संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या
(c) आखिरी संवाद और जीवन यात्रा
(d) मुक्ति और नया युग
Correct Answer : (b) संयुक्त राष्ट्र-संघ और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या
3. भीड़ में खोया आदमी कहानी में मुख्य समस्या क्या है?
(a) गरीबी
(b) बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या
(c) राजनीति
(d) शिक्षा
Correct Answer : (b) बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या
4. कहानी में लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत किस प्रकार के व्यक्ति हैं?
(a) आलसी और लापरवाह
(b) परिश्रमी, ईमानदार और सीधे-सादे
(c) अभिमानी
(d) केवल व्यापारी
Correct Answer : (b) परिश्रमी, ईमानदार और सीधे-सादे
5. कहानी में लेखक को यात्रा के दौरान क्या समस्या पेश आती है?
(a) यात्री का सामान खो जाना
(b) ट्रेन में सीट की कमी और अत्यधिक भीड़
(c) गाड़ी का समय बदलना
(d) रास्ते में दुर्घटना
Correct Answer : (b) ट्रेन में सीट की कमी और अत्यधिक भीड़
6. श्यामलाकांत के बड़े बेटे दीनानाथ को कितने वर्षों से नौकरी की तलाश थी?
(a) 1 वर्ष
(b) 2 वर्ष
(c) 3 वर्ष
(d) 5 वर्ष
Correct Answer : (b) 2 वर्ष
7. कहानी में लेखक ने किस शहर के बेरोजगारी की स्थिति को बताया है?
(a) मुंबई
(b) दिल्ली
(c) लखनऊ
(d) छोटा शहर
Correct Answer : (d) छोटा शहर
8. श्यामलाकांत के घर में लेखक को क्या देखने को मिलता है?
(a) साफ-सुथरा घर
(b) बच्चों की भीड़ और सामान से भरा हुआ घर
(c) सुखी परिवार
(d) बहुत सा धन
Correct Answer : (b) बच्चों की भीड़ और सामान से भरा हुआ घर
9. लेखक के अनुसार श्यामलाकांत की पत्नी की हालत कैसी थी?
(a) स्वस्थ और खुश
(b) दुखी और कमजोर
(c) बीमारी से परेशान
(d) समृद्ध
Correct Answer : (b) दुखी और कमजोर
10. कहानी में श्यामलाकांत की पत्नी ने क्या बताया कि उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा पा रहे थे?
(a) डॉक्टर बहुत महंगे हैं
(b) डॉक्टर की फीस बढ़ गई है
(c) डॉक्टर के पास बहुत भीड़ है
(d) डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं
Correct Answer : (c) डॉक्टर के पास बहुत भीड़ है
11. श्यामलाकांत के छोटे बेटे सुमंत को किस कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा?
(a) पढ़ाई में कमी
(b) रोजगार की कमी
(c) राशन की दुकान पर अत्यधिक भीड़
(d) घर में तनाव
Correct Answer : (c) राशन की दुकान पर अत्यधिक भीड़
12. लेखक का यह सवाल था कि हम किसके लिए जिम्मेदार हैं?
(a) बेरोजगारी
(b) बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण
(c) नदियों की सफाई
(d) राजनीतिक संकट
Correct Answer : (b) बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण
13. कहानी में लेखक का मुख्य विचार क्या था?
(a) केवल शिक्षा की महत्ता
(b) देश की बढ़ती जनसंख्या और उसकी समस्याएँ
(c) सामाजिक संरचना
(d) धर्म और समाज
Correct Answer : (b) देश की बढ़ती जनसंख्या और उसकी समस्याएँ
14. लख के अनुसार बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं?
(a) राजनीतिक अस्थिरता
(b) शिक्षा का संकट
(c) भीड़, बेरोजगारी, और दुर्घटना
(d) धन की कमी
Correct Answer : (c) भीड़, बेरोजगारी, और दुर्घटना
15. कहानी में लेखक किस प्रकार के परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं?
(a) केवल आर्थिक परिवर्तन
(b) केवल सामाजिक परिवर्तन
(c) पर्यावरणीय और जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएँ
(d) राजनीतिक परिवर्तन
Correct Answer : (c) पर्यावरणीय और जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएँ
16. कहानी के अंत में लेखक ने किस विषय पर चिंता जताई?
(a) बेरोजगारी
(b) बढ़ती जनसंख्या और समस्याओं के समाधान की आवश्यकता
(c) राजनीति
(d) शिक्षा
Correct Answer : (b) बढ़ती जनसंख्या और समस्याओं के समाधान की आवश्यकता
17. कहानी में लेखक ने किसका उदाहरण दिया ताकि हमें परिवार के अच्छे प्रबंधन पर विचार करना चाहिए?
(a) श्यामलाकांत का अनियोजित परिवार
(b) उनके अपने परिवार का उदाहरण
(c) एक दूसरे दोस्त का उदाहरण
(d) समाज का उदाहरण
Correct Answer : (a) श्यामलाकांत का अनियोजित परिवार
18. कहानी में लेखक के क्या विचार थे कि भविष्य में क्या हो सकता है?
(a) देश का विकास होगा
(b) बढ़ती जनसंख्या की समस्याएँ बढ़ सकती हैं
(c) बेरोजगारी खत्म हो जाएगी
(d) स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ेंगी
Correct Answer : (b) बढ़ती जनसंख्या की समस्याएँ बढ़ सकती हैं
19. कहानी का संदेश क्या है?
(a) शिक्षा की आवश्यकता
(b) बेरोजगारी पर ध्यान देना
(c) बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान
(d) राजनीतिक मुद्दों पर विचार करना
Correct Answer : (c) बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान
(i) उम्र में मुझ से छोटे हैं, पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है।'
(क) उम्र में कौन, किससे छोटा है? दोनों के नाम बताएँ और आपस में दोनों का क्या संबंध है ?
उत्तर- उम्र में लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत लेखक से छोटे हैं। लेखक का नाम लीलाधर शर्मा पर्वतीय हैं और उनके मित्र का नाम बाबू श्यामलाकांत है। दोनो घनिष्ठ (गहरे) मित्र हैं।
(ख) किसने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है? उसकी चरित्रगत विशेषताएँ लिखें।
उत्तर- लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत ने अपने घर में बच्चों की एक फौज खड़ी कर ली है। वे बहुत ही सीधे-सादे, परिश्रमी (मेहनती) और ईमानदार व्यक्ति है, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। उनका परिवार बड़ा परिवार हैं। अपने अनियोजित परिवार के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
(ग) बच्चों की फौज से क्या तात्पर्य है ? उन्हें वह परिवार 'बच्चों की फौज' क्यों लगता है ?
उत्तर- बच्चों की फौज का अर्थ है कि बहुत बड़ा और अनियोजित परिवार । श्यामलाकांत की बड़ी लड़की की शादी है। उनका एक बेटा पढाई पूरी करके नौकरी की तलाश में भटक रहा है । एक लड़का घर के कामकाज में मदद करता है। उनकी तीन छोटी लड़कियाँ और दो छोटे लड़के है। इसलिए लेखक को श्यामलाकांत का परिवार बच्चों की फौज जैसा प्रतीत हुआ।
(घ) क्या उसका परिवार एक सुखी परिवार है ? कैसे ?
उत्तर- नहीं, उसका परिवार एक सुखी परिवार नहीं है क्योंकि उसकी आमदनी के साधन सीमित हैं। इतने बड़े परिवार में रहन-सहन व खान-पान की उचित व्यवस्था नहीं हैं। बड़े परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, जिसका इलाज ठीक से नहीं' हो पाता हैं। कोई न कोई परि परेशानी उन्हें घेरे रहती हैं।
(ii) 'भाई, नाम तो तुम्हारा लिख लेता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना।'
(क) यह पंक्ति कौन, किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है ?
उत्तर- यह पंक्ति रोजगार दफ़्तर का अधिकारी बाबू श्यामलाकांत के बड़े लड़के दीनानाथ से कह रहा है जब वह दफ्तर में अपना नाम लिखाने के लिए गया था। रजिस्टर में नाम लिखने के बाद अफ़सर ने साथ में यह भी कह दिया कि जल्दी नौकरी पाने को आशा मत रखना क्योंकि उसकी योग्यता के हज़ारों' लोग पहले से ही कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं।
(ख) उसे नौकरी खोजते कितने वर्ष हो गए ? उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही ?
उत्तर- दीनानाथ को नौकरी खोजते हुए दो वर्ष हो गए थे। उसे नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी योगता के हज़ारों लोग पहले से ही रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। पहले उन्हें नौकरी मिलेगी, फिर उसकी बारी आएँगी।
(ग) इस पंक्ति में लेखक ने देश की किस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कैसे ?
उत्तर- इस पंक्ति में लेखक ने तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया हैं। देश की तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश के हर क्षेत्र में भीड़, अनुशासनहीनता, अव्यवस्था, कुपोषण आदि परेशानियों को जन्म दिया है। इसके लिए हमे शीघ्र ही बढती हुई जनसंख्य पर रोक लगानी होगी ।
(घ) इस समस्या के समाधान के लिए कोई दो बिंदु लिखें।
उत्तर- अगर देश को परेशानियों से बचाना है तो जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा अत: इस समस्या के समाधान के लिए दो बिंदु निम्नलिखित है-
1. जनसंख्या को बेहताशा बढ़ने से रोकना होगा
2. परिवार नियोजन की शिक्षा प्रत्येक नागरिक को दी जाए।
(iii) 'क्या तुम्हारे पास यही दो कमरे हैं ?'
(क) यह पंक्ति किसने, किससे कही और क्यों कही ?
उत्तर- यह पंक्ति लेखक ने अपने मित्र श्यामलाकांत से कहाँ जब लेखक अपने मित्र की बड़ी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि मित्र के छोटे-से दो कमरों वाले मकान में सामान भरा पड़ा है और बच्चों की भीड़ है। वहाँ लेखक का दम घुटने लगा है इसलिए लेखक ने अपने मित्र से यह बात कहीं।
(ख) इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कौन-सी परेशानी बताई ?
उत्तर- श्यामलाकांत ने बताया कि वह दो वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहे है। शहर में चक्कर काट-काटकर उनके जुते घिस गए थे। वर्तमान में शहर के बढ़ जाने के बाद भी मकानों की बहुत कमी है। तब बड़ी मुश्किल से उन्हें मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर एक छत मिली हैं।
(ग) उन दो कमरों में कितने लोग रहते हैं ? उनका विवरण दें।
उत्तर- उन दो कमरों में लेखक के मित्र बाबू श्यामलाकांत, उनकी पत्नी, श्यामलाकांत का बड़ा लड़का दीनानाथ, श्यामलाकांत की बड़ी बेटी जिसका विवाह होने वाला है, एक अन्य बेटा सुमंत, तीन छोटी लडकियाँ और दो छोटे लड़के। इस प्रकार दो कमरों में कुल मिलाकर दस लोग रहते हैं।
(घ) इस पंक्ति से किस समस्या की ओर संकेत किया गया है ?
उत्तर- इस पंक्ति में लेखक ने बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की समस्या की और संकेत किया है। देश की जनसंख्या बहुत तेजी से और लगातार बढ़ते जाने के कारण शहर दूर-दूर तक फैलते जा रहे हैं। नई कॉलोनियाँ बन गई है, परंतु फिर भी लोग मकानों लिए भटक रहे हैं।
(iv) 'कब से अस्वस्थ हैं? डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या ?'
(क) यह पंक्ति किसने, किससे कही और क्यों कही ?
उत्तर- यह पंक्ति लेखक ने श्यामलाकांत की पत्नी से कही जब श्यामलाकांत की पत्नी जलपान लेकर आई। तब उनके पीछे तीन छोटी लड़कियाँ और पटला पकडे दो छोटे लड़के थे। लेखक उनकी दुर्बल (कमज़ोर) काया (शरीर) और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया इसलिए उसने यह बात श्यामलाकांत जी की पत्नी से कही।
(ख) इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने किस परेशानी का उल्लेख किया ?
उत्तर- इस प्रश्न के उत्तर में श्यामलाकांत जी की पत्नी ने बताया कि इतने बड़े परिवार में रोज़ कोई न कोई बीमार रहता ही है। उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर को दिखाने गई थी, परन्तु आजकल अस्पतालों में इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर भी मरीजों को ठीक से देख ही नहीं पाते।
(ग) व्यक्ति बीमार किन कारणों से होता है? कोई दो कारण बताएँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?
उत्तर- व्यक्ति बीमार कुपोषण से तथा गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण के कारण होता हैं। इसके लिए हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या मुख्य रूप से जिम्मेवार है। पौष्टिक भोजन और स्वच्छ वातावरण न मिलने के कारण व्यक्ति बीमार होता है।
(घ) बीमारियों से बचने के कोई दो उपाय बताएँ।
उत्तर- यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर पौष्टिक भोजन सामग्री हो, तो बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें गंदगी और दूषित वातावरण से बचना चाहिए तथा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए।
(v) 'मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है।'
(क) 'मुझे' शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ? उन्हें अपने मित्र को किस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है और क्यों ?
उत्तर- ‘मुझे' शब्द लेखक लीलाधर शर्माजी के लिए प्रयुक्त हुआ है। उन्हें अपने मित्र को भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने घर में बच्चों को फ़ौज खड़ी कर ली है। बड़े परिवार के कारण उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं।
(ख) श्यामलाकांत को अपने घर में भीड़ के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?
उत्तर- अपने अनियोजित परिवार के कारण श्यामलाकांत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके आय के साधन कम होने के कारण बच्चों के पालन-पोषण, रहन-सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी सुव्यवस्था नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप उसके परिवार में कोइ न कोई बीमार रहता है और धन की कमी के कारण ठीक प्रकार से इलाजा भी नहीं हो पाता ।
(ग) 'भीड़' शब्द से देश की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है ? इस समस्या के कारण किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ?
उत्तर- ‘भीड़’ शब्द से देश की बढ़ती जनसंख्य की ओर संकेत हैं। देश में जनसंख्या की वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं। अन्न उत्पादन जनसंख्या की अपेक्षा कम होता है। इससे महँगाई और बेरोजगारी बढ़ती है। रोजगार सीमित लोगों को ही मिलपाता है। गरीबी बढ़ती हैं। यदि समय रहते इनसे छुटकारा न पाया गया, तो मनुष्य इन समस्याओं में पूरी तरह खो जाऐगा।
(घ) 'भीड़' से पैदा होने वाली समस्याओं से किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है ?
उत्तर- जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार को सीमित रखना सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बीमारी कुपोषण, अन्यवस्था, अनुशासनहीनता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर देश की इन परेशानियों से बचना है तो जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। परिवार नियोजन की शिक्षा प्रत्येक नागरिक को दी जाए। महिलाओं की स्थिति में सुधार होना चाहिए।
1. लीलाधर शर्मा पर्वतीय कौन थे?
उत्तर- लीलाधर शर्मा पर्वतीय हिंदी साहित्य के लेखक थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा में एक किसान परिवार में हुआ। वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। काशी विद्यापीठ से शास्त्री परीक्षा पास की और हिंदी समिति के लिए काम किया। उनकी लेखन शैली सरल और सुबोध थी। उनकी प्रमुख रचनाएँ 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' और 'स्वतंत्रता की पूर्व संध्या' हैं।
2. 'भीड़ में खोया आदमी' कहानी का सार क्या है?'
उत्तर- भीड़ में खोया आदमी' कहानी बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं को दर्शाती है। लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत के घर जाते हैं और रास्ते में ट्रेन व स्टेशन पर भारी भीड़ का सामना करते हैं। श्यामलाकांत का परिवार अनियोजित है। उनका बेटा दीनानाथ बेरोजगार है। घर में बच्चों और सामान की भीड़ से लेखक परेशान हो जाते हैं। कहानी बताती है कि जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, भीड़ और प्रदूषण बढ़ता है, जिससे व्यक्ति भीड़ में खो जाता है।
3. कहानी का मुख्य पात्र कौन है?
उत्तर- कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं हैं। वे श्यामलाकांत के घर जाते हैं और भीड़ से जूझते हैं। वे संवेदनशील और चिंतनशील हैं। ट्रेन, स्टेशन और श्यामलाकांत के घर की भीड़ देखकर वे जनसंख्या वृद्धि और उससे होने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं। उनका चरित्र समाज की समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति का प्रतीक है।
4. श्यामलाकांत का चरित्र कैसा है?
उत्तर- श्यामलाकांत एक सीधा-सादा, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति है। उनका परिवार बड़ा और अनियोजित है, जिससे घर में अव्यवस्था रहती है। वे अपने बेटे दीनानाथ की बेरोजगारी से चिंतित हैं। उनका चरित्र एक सामान्य मध्यमवर्गीय व्यक्ति को दर्शाता है, जो जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक समस्याओं से प्रभावित है।
5. कहानी में जनसंख्या वृद्धि की क्या समस्याएँ दिखाई गई हैं?
उत्तर- कहानी में जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, भीड़ और प्रदूषण की समस्याएँ दिखाई गई हैं। ट्रेन और स्टेशन पर अत्यधिक भीड़, श्यामलाकांत के बेटे को नौकरी न मिलना, अस्पतालों में लंबी कतारें और दर्जी का काम पूरा न कर पाना, ये सभी समस्याएँ जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं।
6. लेखक को श्यामलाकांत के घर में कैसा अनुभव हुआ?
उत्तर- लेखक को श्यामलाकांत के घर में दम घुटने का अनुभव हुआ। घर में बच्चों और सामान की भीड़ थी। श्यामलाकांत की पत्नी ने बताया कि डॉक्टर के पास जाना और कपड़े सिलवाना भी मुश्किल है क्योंकि हर जगह भीड़ होती है। यह सब देखकर लेखक जनसंख्या की समस्या पर चिंतित हो गए।
7. कहानी का उद्देश्य क्या है?
उत्तर- कहानी का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं पर ध्यान दिलाना है। यह दर्शाती है कि अनियंत्रित जनसंख्या से बेरोजगारी, भीड़ और अव्यवस्था बढ़ती है। कहानी हमें परिवार नियोजन और समाज की भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देती है।
8. दीनानाथ की क्या समस्या थी?
उत्तर- दीनानाथ, श्यामलाकांत का बेटा, दो साल से बेरोजगार है। वह नौकरी की तलाश में भटक रहा है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा। उसकी समस्या छोटे शहरों में बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाती है और जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को उजागर करती है।
9. कहानी का संदेश क्या है?
उत्तर- कहानी का संदेश है कि बढ़ती जनसंख्या समाज के लिए खतरा है। यह बेरोजगारी, भीड़ और प्रदूषण को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति भीड़ में खो जाता है। हमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए, वरना भविष्य में समस्याएँ और गंभीर हो जाएँगी।
10. लेखक ने भविष्य के लिए क्या चिंता व्यक्त की?
उत्तर- लेखक ने चिंता जताई कि यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो एक दिन हम सब भीड़ और उससे होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएँगे। रेलवे स्टेशन, बसें, अस्पताल और अन्य जगहों पर भीड़ बढ़ेगी, जिससे जीवन और कठिन हो जाएगा।

No comments:
Post a Comment